The Hindu Editorial Analysis in Hindi
11 November 2025
COP30 से दक्षिण एशिया क्या चाहता है?
(Source – The Hindu, International Edition – Page No. – 8)
विषय: सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III: पर्यावरण – जलवायु परिवर्तन | सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II: भारत के हितों को प्रभावित करने वाले क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और समझौते
संदर्भ
पेरिस समझौते (2015) के एक दशक बाद भी जलवायु संकट और गहरा गया है — दक्षिण एशिया लगातार मानसूनी बाढ़, भूस्खलन, भीषण गर्मी और बढ़ते समुद्री स्तर जैसी आपदाओं का सामना कर रहा है।
जब विश्व समुदाय ब्राज़ील में आयोजित होने वाले COP30 (2025) की तैयारी कर रहा है, यह आवश्यक है कि दक्षिण एशियाई देश मिलकर जलवायु अनुकूलन, क्षेत्रीय सहयोग तथा न्यायसंगत वित्तपोषण के मुद्दों पर नेतृत्व प्रदर्शित करें।
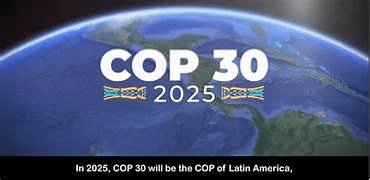
दक्षिण एशिया की जलवायु चिंताएँ
1. जलवायु आपदाओं के प्रति संवेदनशीलता
दक्षिण एशिया की भौगोलिक स्थिति इसे विश्व के सबसे अधिक जलवायु-संवेदनशील क्षेत्रों में से एक बनाती है। यहाँ लगभग दो अरब लोग बाढ़, हिमनद-पिघलाव और सूखे जैसी आपदाओं की चपेट में हैं।
2. बहुपक्षवाद की कमजोरी
संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे वैश्विक शक्तियों के जलवायु प्रतिबद्धताओं से पीछे हटने से अंतरराष्ट्रीय सहयोग की परीक्षा हुई है, जिससे अब छोटे देशों पर नेतृत्व का भार बढ़ गया है।
3. कार्यान्वयन की कमी
यद्यपि अनेक घोषणाएँ और वादे किए गए हैं, परंतु उनका क्रियान्वयन अपर्याप्त रहा है। वित्तीय वादों और वास्तविक वितरण के बीच की खाई ने आपसी विश्वास को कमजोर किया है।
COP30 में दक्षिण एशिया की प्राथमिकताएँ
1. कार्यान्वयन और वित्त
प्रतिज्ञाओं और परिणामों के बीच की दूरी को कम करना अत्यंत आवश्यक है। देशों को वैश्विक अनुकूलन लक्ष्य (Global Goal on Adaptation – GGA) तथा हानि एवं क्षति कोष (Loss and Damage Fund) की मज़बूत रूपरेखा पर स्पष्टता चाहिए।
2. क्षेत्रीय जलवायु सहयोग
दक्षिण एशिया को आपदा-सहनशीलता, तकनीकी साझेदारी और सीमा-पार सहयोग को सुदृढ़ करना होगा।
भारत की आपदा-सहनशील अवसंरचना के लिए गठबंधन (CDRI) और सगरमाथा संवाद (Sagarmatha Sambhad) जैसे उपक्रम इस दिशा में सकारात्मक उदाहरण हैं।
3. अनुकूलन और शमन का समन्वय
क्षेत्र को जलवायु-सहनशील कृषि, अक्षय ऊर्जा विकास और तटीय सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
4. समावेशी और पारदर्शी शासन
स्थानीय समुदायों, महिलाओं और अल्प-प्रतिनिधित समूहों को जलवायु निर्णय-प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल किया जाना चाहिए।
5. निजी क्षेत्र और गैर-राज्यीय अभिकर्ता
COP30 में निजी कंपनियों, नागरिक समाज संगठनों और तकनीकी नवाचार संस्थाओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और मिश्रित वित्तपोषण (blended finance) के माध्यम से जलवायु-कार्य को गति दी जा सके।
दक्षिण एशिया को आवश्यक सहयोग
1. तकनीकी और संस्थागत क्षमता
जलवायु आँकड़ा-निगरानी, जोखिम मूल्यांकन और अनुकूलन-योजनाओं के लिए घरेलू संस्थागत तैयारी को मज़बूत किया जाए।
2. वित्तीय प्रतिबद्धताएँ
विकसित देशों को हरित जलवायु कोष (Green Climate Fund) और अनुकूलन कोष (Adaptation Fund) जैसे माध्यमों से पूर्वानुमेय, पारदर्शी और सुलभ वित्तपोषण सुनिश्चित करना चाहिए।
3. विश्वास निर्माण
जलवायु वित्त न्यायसंगत, पारदर्शी और समावेशी होना चाहिए ताकि विकासशील देशों का विश्वास बहाल हो सके।
आगे की राह
- दक्षिण एशियाई लचीलापन वित्त सुविधा (South Asian Resilience Finance Facility) की स्थापना की जाए, जिससे क्षेत्रीय स्तर पर अनुकूलन और शमन कार्यक्रमों को सहायता मिले।
- डिजिटल एवं डाटा अवसंरचना को मज़बूत बनाया जाए ताकि जलवायु-प्रगति का सटीक मूल्यांकन हो सके।
- हरित प्रौद्योगिकी, शीघ्र चेतावनी तंत्र और तटीय-सुरक्षा पर क्षेत्रीय समझौते (regional compacts) को बढ़ावा दिया जाए।
निष्कर्ष
दक्षिण एशिया वैश्विक जलवायु संकट की अग्रपंक्ति में खड़ा है। COP30 में इस क्षेत्र को केवल पीड़ित की भूमिका से आगे बढ़कर नेतृत्वकारी भूमिका निभानी होगी —
जहाँ वित्त में न्याय, शासन में समावेशिता, और क्षेत्रीय एकता इसकी पहचान बने।
“COP30 में दक्षिण एशिया की आवाज़ ऐसी होनी चाहिए जो संवेदनशीलता और दृष्टि दोनों को प्रतिबिंबित करे —
सहयोग पर आधारित लचीलापन, और सतत विकास पर आधारित प्रगति।”


